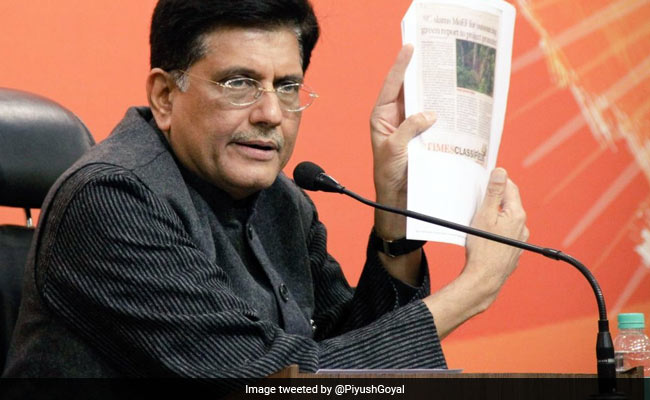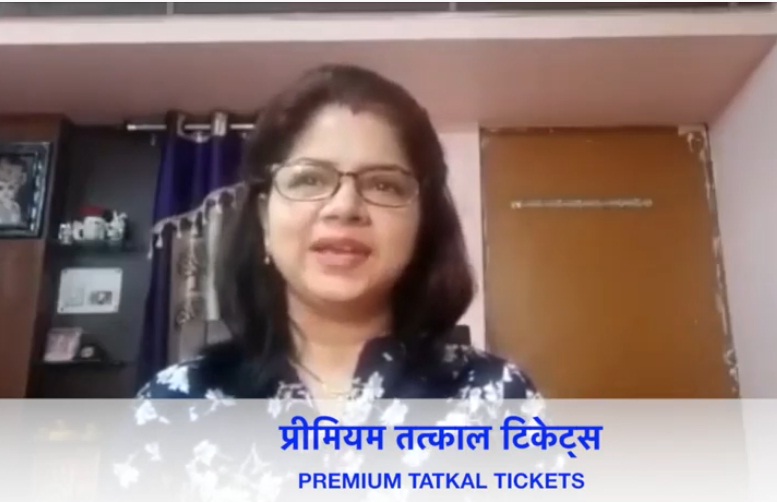क्या होता है जब हीन भावना से ग्रस्त और प्रतिकूल परिस्थितियों से पस्त कोई दीन-हीन ऐसा किशोर कॉलेज परिसर में दाखिल हो जाता है जिसने मेधावी होते हुए भी इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी कि अपनी शिक्षा – दीक्षा को वह कभी कॉलेज के स्तर तक पहुंचा पाएगा? क्या कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ना ऐसे अभागे नौजवानों के लिए सहज होता है? क्या वहां उसे उसके सपनों को पंख मिल पाते हैं या फिर महज कुछ साल इस गफलत में बीत जाते हैं कि वो भी कॉलेज तक पढ़ा है? ….अपने बीते छात्र जीवन के पन्नों को जब भी पलटता हूं तो कुछ ऐसे ही ख्यालों में खो जाता हूं. क्योंकि पढ़ाई में काफी तेज होते हुए भी बचपन में ही मैने कॉलेज का मुंह देख पाने की उम्मीद छोड़ दी थी. कोशिश बस इतनी थी कि स्कूली पढ़ाई पूरी करते हुए ही किसी काम – धंधे में लग जाऊं. पसीना पोंछते हुए पांच मिनट सुस्ताना भी जहां हरामखोरी मानी जाए, वहां सैर-सपाटा, पिकनिक या भ्रमण जैसे शब्द भी मुंह से निकालना पाप से कम क्या होता.

जल्द ही मेरे पांव वास्तविकता की जमीन पर थे. 354 नाम की जिस पैसेंजर ट्रेन से हम घाटशिला जाते थे, वह सामाजिक समरसता और सह – अस्तित्व के सिद्धांत की जीवंत मिसाल थी. क्योंकि ट्रेन की अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के कुछ देर बाद ही लकड़ी के बड़े – बड़े गट्ठर, मिट्टी के बने बर्तन और पत्तों से भरे बोरे डिब्बों में लादे जाने लगते. खाकी वर्दी वाले डिब्बों में आते और कुछ न कुछ लेकर चलते बनते. यह हकीकत आज भी यथावत है.
लेकिन उस दौर में भी कुछ भ्रमण प्रेमियों के हवाले से उस खूबसूरत कस्बे घाटशिला का नाम सुना था. ट्रेन में एकाध यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की खिड़की से कस्बे की हल्की सी झलक भी देखी थी. लेकिन चढ़ती उम्र में ही इस शहर से ऐसा नाता जुड़ जाएगा जो पूरे छह साल तक बस समय की आंख – मिचौली का बहाना बन कर रह जाएगा यह कभी सोचा भी न था. यह भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के खुद को संभालने की कोशिश के दरम्यान की बात है. होश संभालते ही शुरू हुई झंझावतों की विकट परिस्थितियों में मैने कॉलेज तक पहुंचने की आस छोड़ दी थी. समय आया तो नए विश्व विद्यालय की मान्यता का सवाल और अपने शहर के कॉलेज में लड़कियों के साथ पढ़ने की मजबूरी ने मुझे और विचलित कर दिया, क्योंकि मैं बचपन से इन सब से दूर भागने वाला जीव रहा हूं.
 इस बीच मुझे अपने शहर से करीब सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित घाटशिला कॉलेज की जानकारी मिली. स्कूली जीवन में अपने शहर के नाइट कॉलेज की चर्चा सुनी थी. लेकिन कोई कॉलेज सुबह सात बजे से शुरू होकर सुबह के ही 10 बजे खत्म हो जाता है, यह पहली बार जाना. अपनी मातृभाषा में कॉलेज की शिक्षा हासिल करना और वह भी इस परिस्थिति में कि मैं अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी पहले की तरह करता रह सकूं, मुझे यह एक सुनहरा मौका प्रतीत हुआ और मैने उस कॉलेज में दाखिला ले लिया. यद्यपि अपनी पसंद के विपरीत इस चुनाव में मुझे कॉमर्स पढ़ना था, फिर भी मैने इसे हाथों हाथ लिया. क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि जीवन में कभी कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ना संभव भी हो पाएगा. चुनिंदा सहपाठियों से तब पता लगा कि तड़के पांच बजे की ट्रेन से हमें घाटशिला जाना होगा और लौटने के लिए तब की 29 डाउन कुर्ला टी – हावड़ा एक्सप्रेस मिलेगी.
इस बीच मुझे अपने शहर से करीब सौ किलोमीटर की दूरी पर स्थित घाटशिला कॉलेज की जानकारी मिली. स्कूली जीवन में अपने शहर के नाइट कॉलेज की चर्चा सुनी थी. लेकिन कोई कॉलेज सुबह सात बजे से शुरू होकर सुबह के ही 10 बजे खत्म हो जाता है, यह पहली बार जाना. अपनी मातृभाषा में कॉलेज की शिक्षा हासिल करना और वह भी इस परिस्थिति में कि मैं अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भी पहले की तरह करता रह सकूं, मुझे यह एक सुनहरा मौका प्रतीत हुआ और मैने उस कॉलेज में दाखिला ले लिया. यद्यपि अपनी पसंद के विपरीत इस चुनाव में मुझे कॉमर्स पढ़ना था, फिर भी मैने इसे हाथों हाथ लिया. क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि जीवन में कभी कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ना संभव भी हो पाएगा. चुनिंदा सहपाठियों से तब पता लगा कि तड़के पांच बजे की ट्रेन से हमें घाटशिला जाना होगा और लौटने के लिए तब की 29 डाउन कुर्ला टी – हावड़ा एक्सप्रेस मिलेगी.
 शुरू में कुछ दिन तो यह बदलाव बड़ा सुखद प्रतीत हुआ. लेकिन जल्द ही मेरे पांव वास्तविकता की जमीन पर थे. 354 नाम की जिस पैसेंजर ट्रेन से हम घाटशिला जाते थे, वह सामाजिक समरसता और सह – अस्तित्व के सिद्धांत की जीवंत मिसाल थी. क्योंकि ट्रेन की अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के कुछ देर बाद ही लकड़ी के बड़े – बड़े गट्ठर, मिट्टी के बने बर्तन और पत्तों से भरे बोरे डिब्बों में लादे जाने लगते. खाकी वर्दी वाले डिब्बों में आते और कुछ न कुछ लेकर चलते बनते. अराजक झारखंड आंदोलन के उस दौर में बेचारे इन गरीबों का यही जीने का जरिया था. वापसी के लिए चुनिंदा ट्रेनों में सर्वाधिक अनुकूल 29 डाउन कुर्लाटी – हावड़ा एक्सप्रेस थी, लेकिन तब यह अपनी लेटलतीफी के चलते जानी जाती थी. यही नहीं ट्रेनों की कमी के चलते टाटानगर से खड़गपुर के बीच यह ट्रेन पैसेंजर के तौर पर हर स्टेशन पर रुक – रुक कर चलती थी. कभी – कभी तब राउरकेला तक चलने वाली इस्पात एक्सप्रेस से भी लौटना होता था.
शुरू में कुछ दिन तो यह बदलाव बड़ा सुखद प्रतीत हुआ. लेकिन जल्द ही मेरे पांव वास्तविकता की जमीन पर थे. 354 नाम की जिस पैसेंजर ट्रेन से हम घाटशिला जाते थे, वह सामाजिक समरसता और सह – अस्तित्व के सिद्धांत की जीवंत मिसाल थी. क्योंकि ट्रेन की अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के कुछ देर बाद ही लकड़ी के बड़े – बड़े गट्ठर, मिट्टी के बने बर्तन और पत्तों से भरे बोरे डिब्बों में लादे जाने लगते. खाकी वर्दी वाले डिब्बों में आते और कुछ न कुछ लेकर चलते बनते. अराजक झारखंड आंदोलन के उस दौर में बेचारे इन गरीबों का यही जीने का जरिया था. वापसी के लिए चुनिंदा ट्रेनों में सर्वाधिक अनुकूल 29 डाउन कुर्लाटी – हावड़ा एक्सप्रेस थी, लेकिन तब यह अपनी लेटलतीफी के चलते जानी जाती थी. यही नहीं ट्रेनों की कमी के चलते टाटानगर से खड़गपुर के बीच यह ट्रेन पैसेंजर के तौर पर हर स्टेशन पर रुक – रुक कर चलती थी. कभी – कभी तब राउरकेला तक चलने वाली इस्पात एक्सप्रेस से भी लौटना होता था.
एक पिछड़े क्षेत्र में किसी ट्रेन के छूट जाने पर किस तरह दूसरी ट्रेन के लिए मुसाफिरों को घंटों बेसब्री भरा इंतजार करना पड़ता है और यह उनके लिए कितनी तकलीफदेह होती है. सफर के दौरान खुद भूख – प्यास से बेहाल होते हुए दूसरों को लजीज व्यंजन खाते देखना, स्टेशनों के नलों से निकलने वाले बेस्वाद चाय सा गर्म पानी पीने की मजबूरी के बीच सहयात्रियों को कोल्ड ड्रिंक्स पीते निहराना यह नीयती आज बहुत खलती है.
भारी भीड़ से बचने के लिए हम छात्र इस ट्रेन के पेंट्रीकार में चढ़ जाते थे. इस आवागमन के चलते बीच के स्टेशनों जैसे कलाईकुंडा, सरडिहा, झाड़ग्राम, गिधनी, चाकुलिया , कोकपारा और धालभूमगढ़ से अपनी दोस्ती सी हो गई. अक्सर मैं शिक्षा को दिए गए मैं अपने छह सालों के हासिल की सोचता हूं तो लगता है भौतिक रूप से भले ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया हो, लेकिन इसकी वजह से मै जान पाया कि एक पिछड़े क्षेत्र में किसी ट्रेन के छूट जाने पर किस तरह दूसरी ट्रेन के लिए मुसाफिरों को घंटों बेसब्री भरा इंतजार करना पड़ता है और यह उनके लिए कितनी तकलीफदेह होती है. सफर के दौरान खुद भूख – प्यास से बेहाल होते हुए दूसरों को लजीज व्यंजन खाते देखना, स्टेशनों के नलों से निकलने वाले बेस्वाद चाय सा गर्म पानी पीने की मजबूरी के बीच सहयात्रियों को कोल्ड ड्रिंक्स पीते निहराना, मारे थकान के जहां खड़े रहना भी मुश्किल हो दूसरों को आराम से अपनी सीट पर पसरे देखना और भारी मुश्किलें झेलते हुए घर लौटने पर आवारागर्दी का आरोप झेलना अपने छह साल के छात्र जीवन का हासिल रहा.
 तारकेश कुमार ओझा, लेखक पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है – 09434453934, 9635221463
तारकेश कुमार ओझा, लेखक पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रहते हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे संपर्क किया जा सकता है – 09434453934, 9635221463